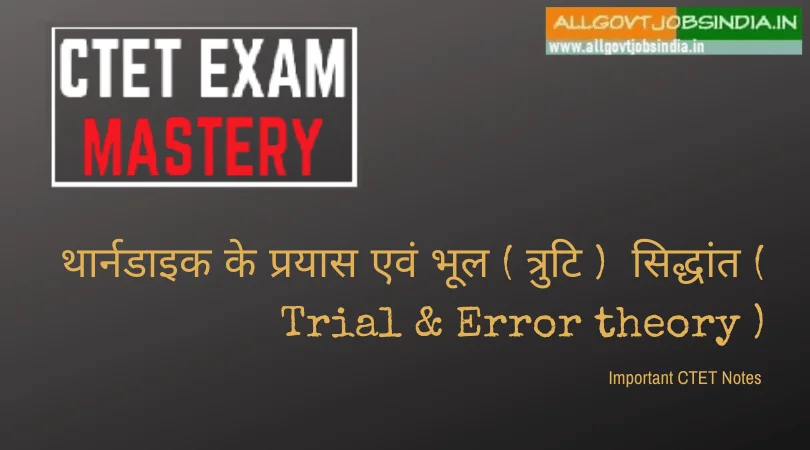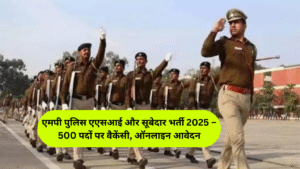( Thorndike Trail and Error Theory )
थार्नडाइक के प्रयास एवं भूल ( त्रुटि ) सिद्धांत ( Trial & Error theory )
इस सिद्धांत को थार्नडाइक ने 1898 में प्रतिपादत किया था। इस सिद्धांत द्वारा उन्हे यह पाता लगया की पशुओं और मानवों को सिखाने में प्रयासों और भूलों का विशेष महत्व है। थार्नडाइक बहुत से प्रयोग जानवरों पर किए जो इस सिद्धांत को साबित करते है। इस सिद्धांत को संयोजनवाद और उद्वीपन – अनुक्रिया का सिद्धांत भी कहां जाता है ।
अधिगम में बहुत से अलग अलग क्रियाओं में सम्बन्ध स्थापित किए जाते हैं तथा सम्बन्ध स्थापना का कार्य हमारा दिमाग करता है जैसे-जैसे हमारी कोशिश बढ़ती है वैसे-वैसे गल्तियां कम होती हैं। इस प्रकार हम अपनी गल्तियों से बहुत कुछ सीखते हैं। इस सिद्धांत में हम बहुत कुध सीखते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार जब कोई जीव नई परिस्थितियों में रखा जाता है तो वह बिना सोचे समझे कई तरह के प्रयास करता है।
यह क्रिया निर्धारक या दोषपूर्ण होती है। जब बार-बार जीभ को उन्हीं हालातों में रखा जाए तो असफल क्रियाएं कम हो जाती हैं, अर्थात जीव या प्राणी अलग अलग ही कोशिशों एवं भूलों के माध्यम से ठीक ठीक करना सीखता है। समस्या के समाधान की प्राप्ति के बाद प्राणी को जो संतुष्टि मिलती है उसके कारण उसे अभी प्रेरणा प्राप्त होती है जिसके परिणाम स्वरुप वह उसी क्रिया को दुबारा दोहराता है तथा असफल विधि को थार्नडाइक ने प्रयास एवं भूल द्वारा सीखने के रूप में परिभाषित किया है।
थार्नडाइक का प्रयोग
- थार्नडाइक द्वारा बिल्ली पर प्रयोग: इस सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए ठंडा एक ने बिल्ली पर एक प्रयोग किया इस प्रयोग से उसने एक उलझन पेटी में भूखी बिल्ली को बंद कर दिया बेटी के बाहर उसने एक मांस का टुकड़ा रख दिया परीक्षण के शुरू होने पर बिल्ली मांस के टुकड़े को प्राप्त करने के लिए उत्पाद ऊधम मचाने लगी उसने दरवाजे खोलने के लिए कई प्रयास किए काफी प्रयासों के बाद उछलकूद के दौरान अचानक बिल्ली का पंजा चिटकनी के ऊपर पड़ गया और पेटी का दरवाजा खुल गया बिल्ली ने बाहर आकर मांस का टुकड़ा खाना शुरु कर दिया दूसरी बार परीक्षण करने पर कुछ समय में बिल्ली ने दरवाजा खोल लिया और अंत में वह एक ही प्रयास में दरवाजा खोलना सीख जाती है।
- लायड़ मार्डन द्वारा किया गया कुते पर प्रयोग: एक कुत्ते को ऐसे लोहे के पिंजरे में बंद कर दिया गया जिसका दरवाजा स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता था। कुत्ते ने कई प्रयास किए और अन्त में दरवाजा खोल लिया।
- मैकङ्यूगल द्वारा चूहे पर किया गया प्रयोग: इस प्रयोग में भी चूहे को एक ऐसे छोटे बक्से में बंद कर दिया गया जिसका रास्ता छुपा हुआ था चूहे ने 165 बार गलतियां करने के पश्चात अंत में ठीक रास्ता ढूंढ लिया।
प्रयास और भूल के प्रयोग के निष्कर्ष ( Conclusion of Trail and Error Experiments) :
यह सभी प्रयोग प्रयत्न और भूल द्वारा सीखने के सिद्धांत की पुष्टि करते हैं कोई भी नया कार्य सीखने में व्यक्ति से शुरू में गलतियां होती है और तब वह ठीक ढंग अपना पता है संगीत के बाजे सीखने में टाइपिंग सीखने में लिखना सीखने में और किसी भी नई परिस्थिति में पड़ जाने पर व्यक्ति को इस विधि का सहारा लेना पड़ता है लेकिन मुख्य रूप से इस प्रकार सीखना व्यापक पैमाने पर शिष्यों और पशुओं में होता है।
इस प्रकार सीखना में व्यापक दशाओं का होना आवश्यक है।
1.पशु या मनुष्य के सामने लक्ष्य स्पष्ट रूप से हो या वह पूर्ण रूप से प्रेरित हो, जैसे बिल्ली के सामने मछली प्राप्त करके अपनी भूख मिटाना।
2. जब व्यक्ति या पशु ऐसी परिस्थिति या समस्या में पड़ जाए कि उसका हाल समझ में ना आता हो।
प्रयास और भूल के सिद्धांत की विशेषताएं
- अधिगम ही संयोजन हैः थार्नडाईक ने अपने प्रयोग से यह निष्कर्ष निकाला कि अधिगम की क्रिया का आधार स्नायुमंडल है। स्नायुमंडल में एक नाड़ी का दूसरी नाड़ी से सम्बन्ध हो जाता है।
- संयोजन सिद्वांत: संयोजन सिद्धांत मनोविज्ञान के क्षेत्र में नवीन विचारधारा तो है ही, साथ ही वह अधिगम का महत्वपर्ण सिद्धांत भी है।
- सम्पूर्ण ईकाई नही: यह मत संयोगों को बहुत महत्त्व देता है। जो व्यक्ति जीवन में अधिक संयोग बना पाता है उतना ही बुद्धिमान कहलाता है।
प्रयास एवं भूल द्वारा सीखने के आवश्यक तत्व
- आभिप्रेरणा: प्रेरणा के अभाव में इस सिद्धांत के अनुसार सीखना कठिन है। किसी प्रकार के तनाव के अभाव में व्यक्ति तत्काल स्वयं को समायोजित करने में सफल हो सकता है। व्यवहार में कोई परिवर्तन नही होता इसलिए प्रेरणा के अभाव में सीखना कठिन होता है।
- बाधा: किसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए बाधा का होना आवश्यक है नहीं तो व्यक्ति कुछ भी नहीं सीख सकता इसी बाधा को दूर करने के प्रयास करके मनुष्य सीखता है।
- निरर्थक अनुक्रियाए: इस प्रयोग के दौरान मनुष्य कुध निरर्थक क्रियाएं करता है, लेकिन यह हमारे लिए सार्थक सिद्ध होती हैं क्योंकि इनसे ही पता चलता है कि हमारी समस्या के समाधान के लिए यह क्रियाए अनुकूल है या नहीं।
- व्यर्थ क्रियाओं को दूर करना: इस सिद्धांत में निरर्थक क्रियाओं गलत और असफल अनु क्रियाओं को एक-एक करके दूर किया जाता है और सही क्रिया की जाती है।
- अचानक सफलता: इस सिद्धांत में अचानक सफल अनुक्रिया का ज्ञान होता है।
- चयन: असफल क्रियाओं में से सही अनुक्रिया का चयन किया जाता है।
- स्थिरता: तेरे प्रयास करते हुए जीव अपनी भूलों को कम करते हुए अनु क्रियाओं के स्थान पर सही अनु क्रियाओं को दिखाना सीख जाते हैं।
प्रयास और मूल सिद्धांत की शैक्षिक उपयोगिता
- काम करके सीखना: यह सिद्धांत विद्यार्थियों को आपने हाथ से काम करके सीखने का मौका देता है।
- सरल से कठिन: इस सिद्धांत के अनुसार अध्यापक विद्यार्थी को सरल से कठिन ज्ञान से अज्ञात और प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर चलने को कहे।
- लक्ष्य- केन्द्रति : हर क्रिया में एक लक्ष्य होता है और मनुष्य उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रयास करता है।
- स्वः अधिकार: इस सिद्धांत के अनुसार विद्यार्थी अपने आप सीखने की कोशिश करते हैं। उनके प्रयास में पहले तो त्रुटियां होती है लेकिन धीरे-धीरे उनकी कमियां कम होने लगती है।
- अभ्यास द्वारा सीखना: यह बात प्रसिद्ध है कि अभ्यास व्यक्ति को कुशल बना देता है अभ्यास के माध्यम से ही शिक्षक बालक को ज्यादा से ज्यादा शिक्षा दे सकते हैं।
- सूझबूझ द्वारा सीखने में प्रयोग: सूज भुज द्वारा सीखने की प्रक्रिया में प्रयास और भूल विधि का समावेश होता है इसके बिना सूज भुज का प्रयोग नहीं हो सकता।
- कौशल का विकास: इस सिद्धांत के द्वारा छात्रों में उनके कौशलों का विकास किया जा सकता है उदाहरण के लिए नाचना, गाना, संगीत सिखाना, टाइप करना आदि।
- अच्छी आदतों का विकास: इस सिद्धांत से बालक में अच्छी आदतें पैदा होती है जैसे बड़ों का आदर करना, धर्य रखना, मेहनत करना, सत्य बोलना बड़ों का आदर करना।
- प्रेरणा का महत्व: ठंडाई के इस सिद्धांत में विद्यार्थियों को अभी प्रेरित करने पर जोर दिया है उसके लिए अध्यापक दंड, प्रशंसा, पुरस्कार आदि की सहायता ले सकता है।
- वैज्ञानिक आधार: विश्व में कई वैज्ञानिक अनुसंधान कार्य प्रयास और भूल के सिद्धांत पर काम करते हैं।
प्रयास और भूल सिद्धांत की सीमाएं
- इस सिद्धांत के अनुसार हर अधिगम संभव नहीं है कई बार बहुत प्रयास करने के बाद भी सफलता नहीं मिलती।
- इस विधि से स्थान नियंत्रण बहुत कम होता है।
- इस विधि में समय और शक्ति बहुत लगती है और व्यर्थ की कोशिशों से समय बेकार जाता है।
- यह एक धीमी गति की प्रक्रिया है इसी कारण प्रतिभाशाली बच्चे इसे कम पसंद करते हैं और मंद बुद्धि वाले बालक अधिक पसंद करते हैं।
- यह एक यांत्रिक विधि है इस विधि से बुद्धि का प्रयोग नहीं किया जाता।
निष्कर्ष
प्रयास और भूल सिद्धांत में दोष होने के बावजूद इस सिद्धांत का बहुत महत्व है इस सिद्धांत में थार्नडाईक ने असफलता को सफलता में बदलने का प्रयास किया है। असफल क्रियाओं में से सही अनुक्रिया का चुनाव किया जाता है। जिससे मनुष्य हर समस्या का समाधान निकाल सकता है।